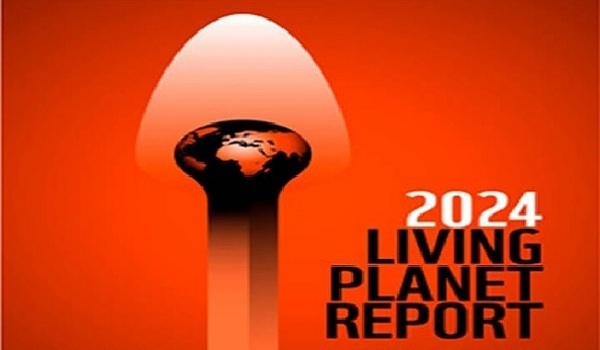वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, केवल 50 वर्षों (1970-2020) में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों (85%) में दर्ज की गई, उसके बाद स्थलीय (69%) और समुद्री (56%) पारिस्थितिकी तंत्र का स्थान रहा।
विश्व वन्यजीव प्रकृति कोष
- यह विश्व का अग्रणी संरक्षण संगठन है और 100 से अधिक देशों में कार्यरत है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विटजरलैंड में है।
- इसका मिशन प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के समक्ष खतरों को कम करना है।
- WWF विश्व भर के लोगों के साथ हर स्तर पर सहयोग करता है ताकि ऐसे नवोन्मेषी समाधान विकसित किये जा सकें जिससे समुदायों, वन्यजीवों एवं उनके निवास स्थानों की रक्षा हो सके।
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (जिसे सामान्यतः WWF-इंडिया के नाम से जाना जाता है) की स्थापना वर्ष 1969 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी।
- यह एक स्वायत्त संरचना के माध्यम से कार्य करता है जिसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं।
लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष
- WWF द्वारा वन्यजीव आबादी में औसत रुझानों को ट्रैक करने के लिये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) का उपयोग किया जाता है। इसमें समय के साथ प्रजातियों की आबादी के आकार में होने वाले व्यापक बदलावों पर नज़र रखी जाती है।
- ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL) द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में वर्ष 1970 से 2020 तक 5,495 प्रजातियों की लगभग 35,000 कशेरुकी आबादी की निगरानी की गई है।
- यह विलुप्त होने के जोखिमों के संदर्भ में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है और पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य एवं दक्षता का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है।
मुख्य निष्कर्ष
- जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट: निगरानी किये गये वन्यजीवों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (95%), अफ्रीका (76%) एवं एशिया-प्रशांत (60%) तथा मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों (85%) में दर्ज की गई है।
- वन्यजीवों के लिये प्राथमिक खतरे: आवास की हानि और क्षरण को विश्व भर में वन्यजीव आबादी के लिये सबसे बड़ा खतरा बताया गया है इसके बाद अतिदोहन, आक्रामक प्रजातियों और रोग को शामिल किया गया है।
- पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक: वन्यजीव आबादी में गिरावट, विलुप्त होने के बढ़ते जोखिम और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की हानि को प्रारंभिक चेतावनी संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र काफी अधिक संवेदनशील होने के साथ अपरिवर्तनीय परिवर्तन की ओर ले जाते हैं।उदाहरण के लिये, ब्राज़ील के अटलांटिक वन में किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि बड़े फल खाने वाले जानवरों की कमी के कारण बड़े बीज वाले वृक्षों के बीजों का फैलाव कम हो गया है, जिससे कार्बन भंडारण प्रभावित हुआ है।WWF ने चेतावनी दी है कि इस घटना से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के वनों में 2-12% कार्बन भंडारण की हानि हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के बीच उनकी कार्बन भंडारण क्षमता कम हो जाएगी।
- क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यता: वर्ष 2030 तक प्रकृति को पुनःस्थापित करने के लिये वैश्विक समझौते और समाधान मौज़ूद हैं, लेकिन अभी तक प्रगति सीमित रही है, तथा तत्परता का अभाव रहा।वर्ष 2030 के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों में से आधे से अधिक के अपने लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना नहीं है, तथा 30% लक्ष्य पूर्व में ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं या उनकी स्थिति वर्ष 2015 की आधार स्तर से भी बदतर है।
- आर्थिक प्रभाव: वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक (55%) भाग मध्यम या अत्यधिक रूप से प्रकृति और उसकी सेवाओं पर निर्भर है।रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत के आहार मॉडल को विश्व भर में अपनाया गया तो वर्ष 2050 तक विश्व को खाद्यान्न उत्पादन के लिये पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता होगी।
विश्व वन्यजीव कोष (WWF)
- यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गयी थी
- मुख्यालय – ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड)
- इसका उद्देश्य वन्यजीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना है
WWF द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट –
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report)
- लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index)
- इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन (Ecological Footprint Calculation)